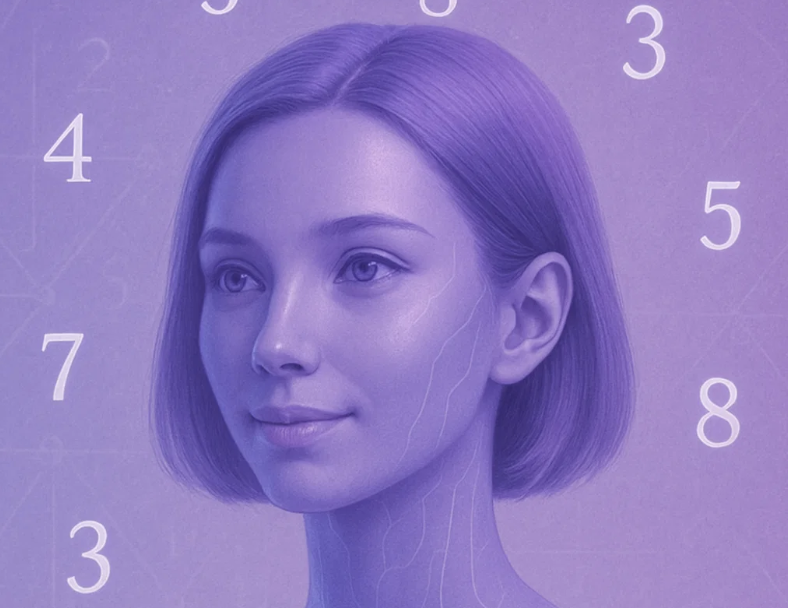कर्मिक संबंध: 9 मुख्य लक्षण, कारण, जन्मतिथियों से गणना और सुधार/समापन की पूर्ण मार्गदर्शिका
साथियों के कर्मिक संबंध क्या होते हैं, उनके लक्षण, वे क्यों उत्पन्न होते हैं, उन्हें कैसे प्रोसेस (समाधान) करें और जन्मतिथियों के आधार पर उनका हिसाब कैसे लगाएं

साथियों के कर्मिक संबंध क्या होते हैं?
जीवन में लोग अक्सर “कर्म” शब्द से रूबरू होते हैं, पर कई बार यह स्पष्ट नहीं होता कि यह क्या है और कर्मिक संबंध क्या होते हैं। कर्म हमारे विचारों, कर्मों, आचरण और अलग-अलग लोगों के साथ संबंधों का समुच्चय है—वे प्रतिक्रियाएं जो हमने इस या पिछली जिंदगी में पैदा कीं। यह सब भविष्य के लिए कर्मिक कार्यों (सीखों) का कारण बनता है या फिर प्रसिद्ध “कर्म में प्लस” लाता है। इसलिए कर्मिक संबंध बहुत सुखद भी हो सकते हैं और समस्याओं का स्रोत भी।
कर्म के निम्न प्रकार हो सकते हैं:
- व्यक्तिगत — प्रत्येक व्यक्ति के लिए निजी।
- अंतरवैयक्तिक — वे संबंध जो जीवन भर मिलने वाले सभी लोगों से बनते हैं, माता-पिता और परिवार के सदस्यों से आरंभ होकर। माता-पिता और बच्चों, पति और पत्नी, मित्रों और सहेलियों के बीच भी अंतरवैयक्तिक कर्मिक कड़ी होती है।
जीवन हमें जिन-जिन लोगों से मिलाती है, वे सभी हमारे कर्मिक साथी हो सकते हैं। यह केवल माता-पिता, बच्चे और नज़दीकी रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि मित्र, परिचित, सहकर्मी आदि भी हैं।
अधूरे संबंध या ऐसे संपर्क जिनसे हमने सही निष्कर्ष नहीं निकाले, वे आत्मा के अगले जन्मों में भी दोहरते हैं। ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के साथ के संबंधों ने आवश्यक सीख नहीं दी, या जिन निष्कर्षों में गलती हुई, वे नए जन्म में फिर से हमारे जीवन में लौट आते हैं। यह नकारात्मक कर्म का परिणाम है।
मनुष्य के जीवन में हर चीज़ कर्म से जुड़ी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा बचपन में माता-पिता की ठंडेपन या क्रूरता से पीड़ित रहा, तो नए जन्म में वही व्यक्ति ऐसे माता-पिता में से एक बन सकता है। यह इसलिए दिया जाता है ताकि वह पिछले जन्म के माता-पिता के व्यवहार के कारणों को समझे, निष्कर्ष निकाले और कर्मिक पाठ सीखे, ताकि गलती न दोहराए।
ऐसी कड़ी को ही कर्मिक बंधन कहा जाता है। ऊर्जाओं की तरह यह भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। कर्म कभी-कभी गलतियों और पाठों की प्रोसेसिंग के लिए भेजी जाती है, तब इसे दंड या कठिन श्रम जैसा महसूस किया जा सकता है। और कभी पुरस्कारस्वरूप भी आती है—जो खुशी, आनंद और सफलता देती है।
कर्मिक संघों के प्रकार
कर्मिक संबंधों को देखते हुए दो प्रकार विशेष रूप से स्पष्ट दिखते हैं: दैविक (सुदैव/नियति-निर्धारित) संघ और दर्पण (मिरर) संघ। इन्हें एक-दूसरे से अलग पहचानना महत्वपूर्ण है।
दैविक (सुदैव) संघ
यह प्रकार उन लोगों में उत्पन्न होता है, जिनमें से एक के कर्मिक “टेल” में आर्काना 3–7–22 (उज़निक — क़ैदी) हो, और दूसरे के में 9–3–21 (नादज़िरातेल — पहरेदार) हो। इन अर्थों को व्यापक अर्थ में समझें। उदाहरण के लिए, संघ का एक सदस्य पिछले जीवन में कैदी था, बंदी था या हानिकारक आदतों—शराब, नशा—का गुलाम था, या रिश्तों/विवाह में अधीनस्थ पक्ष था। दूसरे ने पिछले जन्म में सत्ता का प्रतिनिधि बनकर किसी की स्वतंत्रता सीमित की, घर का तानाशाह, सत्ताधारी बॉस या मनोविज्ञान से नियंत्रक (मैनिपुलेटर) रहा।
ऐसे संघ में जरूरी है कि कर्मिक कार्यों और पाठों की प्रोसेसिंग हो, ताकि पुराने जीवन की स्थितियां नए जन्म में न दोहरें या न बिगड़ें। “क़ैदी” को परिस्थितियों या अन्य लोगों का दास होना बंद करना चाहिए, और “पहरेदार” को नियंत्रण ढीला करना चाहिए—जीवनसाथी/साथी की स्वतंत्रता सीमित न करे।
ऐसे संघ में स्वयं के प्रति ईमानदार रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि दैविक संघ किसी व्यक्ति को अनुकूल लगता है तो क्यों नहीं। पर यदि ऐसे संबंध अस्वीकार और असुविधा उत्पन्न करें—तो उचित कदम उठाने चाहिए। “पहरेदार” को “लगााम ढीली” करनी चाहिए, और “क़ैदी” को केवल परिवार का सदस्य ही नहीं, बल्कि पेशेवर और सामाजिक क्षेत्र में भी स्वयं को साकार करना चाहिए।
दर्पण (मिरर) संघ
नाम से स्पष्ट है—ऐसे संघ में दोनों साथी एक-दूसरे का दर्पण होते हैं। यह तब होता है जब पुरुष और महिला—दोनों में समान प्रमुख आर्काना हावी हों। परिणामस्वरूप, हर कोई “कंबल अपनी ओर खींचता” है—कोई झुकता नहीं, दोनों साबित करना चाहते हैं कि वे दूसरे से अच्छे, बड़े और अधिक महत्वपूर्ण हैं। तब यह संघ नहीं, बल्कि शक्ति-परीक्षा, टकराव और संघर्ष बन जाता है। इसमें तनाव और असुविधा बनी रहती है, इसलिए इस पर कार्य करना अनिवार्य है।
पेशेवर भूमिकाओं को घर पर न थोपना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, महिला—अध्यापिका है। वह विद्यार्थियों को निर्देशित और नियंत्रित करने की आदी है, कई बार अपने अधिकार और ज्ञान से दबा देती है। यदि वही तरीका घरवालों पर लागू होगा, तो परिवार में संकट पनपना आसान है। ऐसी महिला को समझना होगा कि घर पर वह पत्नी, मां, बेटी है—शिक्षक नहीं। उसे “लगााम ढीली” करनी चाहिए; घर में किसी को उपदेश देने/काबू में रखने की जरूरत नहीं—यहां बुद्धिमानी से नीति चलाना, स्त्रैणता और मातृत्व-संवेदना दिखाना पर्याप्त है।
यही बात पुरुष पर भी लागू होती है। यदि वह काम पर बड़ा अधिकारी है, तो इसका मतलब नहीं कि घर पर भी वह अपनों के साथ अधीनस्थों जैसा व्यवहार करे। दर्पण संघ में ऐसी हर कोशिश पर प्रतिबिंबित प्रतिक्रिया मिलती है—साथी लगातार सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं, अपना अधिकार जताते रहते हैं।
दर्पण संघ में सामंजस्य लाने के लिए पुरुष और महिला—दोनों को साथी में अपना ही प्रतिबिंब देखना सीखना होगा। जब वे समझ लेंगे कि उनकी भूलें क्या हैं, तब ऐसे संघ में संतुलन संभव है।
कर्मिक संबंध हैं या नहीं—कैसे पहचानें
कर्मिक कड़ी के निम्नलिखित संकेत होते हैं:
- साथी के पास रहने की निरंतर चाह। लोग या तो विवाह करना चाहते हैं, या साथ में उद्यम/बिज़नेस/प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कभी-कभी इसी संघ में, इसी साथी से बच्चा चाहने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसे भाव मदहोश कर देते हैं, “दिमाग बंद” कर देते हैं—बस वही विचार आते हैं। पर जब लक्ष्यित कर्मिक कार्य पूरा हो जाता है—जैसे प्रोजेक्ट समाप्त होना या बच्चे का जन्म—तो संघ टूट भी सकता है। इसका अर्थ हो सकता है कि कर्मिक कार्य पूरा हो गया, या वह पूरी तरह नहीं हुआ—उदाहरणतः प्रोजेक्ट का अगला चरण होना चाहिए था या बच्चे के जन्म के बाद विधिवत विवाह होना चाहिए था।
- साथियों की उम्र में 10+ वर्ष का अंतर। अलग पीढ़ियों के लोग कर्मिक ऋण की प्रोसेसिंग के लिए साथ हो सकते हैं। ऐसा संघ दर्पण भी हो सकता है और दैविक भी; “शिक्षक” जरूरी नहीं कि उम्र में बड़ा ही हो। इस तरह के कर्मिक संबंध महत्वपूर्ण पाठ देने के लिए भी मिलते हैं और पुरस्कारस्वरूप भी।
- संतान की इच्छा होने पर भी संतान का अभाव। यह किसी अप्रस्फुटित कर्मिक कार्य की मौजूदगी दिखा सकता है। सकारात्मक समाधान से दो परिणाम संभव हैं—लंबे समय से चाहा गया संतान-प्राप्ति, या जोड़ी का अलग होना ताकि आगे के संबंधों में उनके बच्चे हो सकें।
- रिश्ते का तीव्र विकास। साथियों को महसूस हो सकता है कि वे “हमेशा से” एक-दूसरे को जानते हैं, या यह पहली नज़र का प्यार है।
- एक या दोनों साथियों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन। ऐसा संघ तब बनता है जब प्रत्येक साथी की भाग्य मैट्रिक्स में 5, 9 और 2 की शांत ऊर्जाएं हों, और संगतता मैट्रिक्स में 4, 7, 11, 13 और 16 हों। अलग-अलग रहने पर ये लोग शांत रहते हैं, पर साथ आने पर उनकी ऊर्जाएं उफान मारती हैं—परिवर्तन, स्थान-परिवर्तन, आस्था-परिवर्तन आदि होते हैं।
- जोड़ी का एक सदस्य पहले से विवाह में हो। अस्वतंत्र साथी के साथ संबंध सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसी कड़ी कर्म को बिगाड़ती है, और सकारात्मक परिवर्तन किसी अन्य योग्य और स्वतंत्र साथी के साथ सामंजस्यपूर्ण संघ दिला सकते हैं।
- निर्भरता। यह विनाशकारी संघ है, जिसमें एक साथी दूसरे के नकारात्मक प्रभावों/कृत्यों के अधीन हो जाता है—जैसे शारीरिक/मानसिक हिंसा, नियंत्रण, आर्थिक दबदबा आदि सहना।
- व्यक्ति विनाशकारी संघ में रहते हुए भी, नकारात्मक परिणाम समझते हुए भी, निष्कर्ष नहीं निकालता—यहां तक कि विवाह/संबंध टूटने के बाद भी। ऐसे साथी कई बार मिलते-बिछुड़ते हैं—एक दुष्चक्र रचते हैं।
- परिवारिक/साझेदारी संबंधों में कठिन संकट। ऐसे संकट या तो विवाह पंजीकरण के क्षण से या साथ रहने की वास्तविक शुरुआत से बनते हैं। संकट के प्रकार:
- पहले वर्ष का।
- तीन–पांच वर्ष का।
- सात वर्ष का साथ।
- दस, तेरह और इक्कीस वर्षों का विवाह।
यदि इन तिथियों के आस-पास असुविधाजनक घटनाएं—एक-दूसरे से असंतोष, झगड़े, आक्रामकता—उभरती हैं, तो ऐसा विवाह कर्मिक पढ़ा जाता है। इसे उन पहलुओं की प्रोसेसिंग के लिए दिया गया है जो संकट के क्षणों में प्रकट होते हैं।
यह प्रश्न उठ सकता है: क्या कर्मिक संबंध सुखी, समृद्ध वैवाहिक संघ में बदल सकते हैं? निश्चय ही—पर तभी, जब दोनों साथी अपने-अपने और साझा कर्मिक पाठ सफलतापूर्वक प्रोसेस (समाप्त) करें।
कर्मिक संबंध कैसे तोड़ें
यह कहना आसान है कि कर्मिक संबंध अवश्य तोड़ देने चाहिए—पर यह पूरी तरह सही नहीं। कभी-कभी अलगाव ही एकमात्र संभव और सही रास्ता होता है। यदि संबंध विकृति की ओर जा रहा हो और मानसिक—कभी शारीरिक भी—विनाश कर रहा हो, तो अलग होना आवश्यक है। लेकिन अलग भी सही ढंग से होना चाहिए, अन्यथा वही परिस्थितियां नए साथी के साथ और आत्मा के नए जन्म में बार-बार दोहरेंगी। उदाहरण है—कांडों, सार्वजनिक आरोपों, झगड़ों, संपत्ति-विभाजन और टूटने के बाद भी लगातार असंतोष के साथ होने वाला तलाक। निम्न कंपन (लो वाइब्रेशन) पर बिछड़ना अत्यंत हानिकारक है—क्योंकि तब भी कर्मिक कार्यों की प्रोसेसिंग करनी ही पड़ेगी।
रिश्ते और परिवार—बहुत गंभीर कार्य हैं, जो उत्कृष्ट परिणाम भी दे सकते हैं और अलगाव भी। कर्म के दृष्टिकोण से, अलगाव “कैसे” होता है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि टूटने के बाद लोग अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, तो उन्होंने कर्मिक पाठ सीख लिए—और असफल संबंधों को दोहराने के लिए अभिशप्त नहीं होंगे।
हर अलगाव में गलती दोनों की होती है—क्योंकि दोनों प्रेम और मधुर संपर्कों को संभाल नहीं सके। जोड़ी का मुख्य कार्य है—मौजूदा संबंध बचाने का प्रयास करना, विवादों के कारण समझना, छोटी बातों को माफ़ करना, साथी को बदलने की जिद न करना, बल्कि पहले स्वयं में परिवर्तन का प्रयास करना। जब एक व्यक्ति बेहतर बनता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवेश पर पड़ता है—जो सैकड़ों, हज़ारों लोग हो सकते हैं।
यदि हर अगले विवाह/संबंध में वही परिस्थितियां और कठिनाइयां दोहरती महसूस हों, तो समस्या साथियों/आसपास के लोगों में नहीं, बल्कि स्वयं व्यक्ति में है। वह उसी मानक पर जीता है जो उसने अभिभावक-परिवार से सीखा या स्वयं गढ़ा। ऐसा व्यक्ति यह समझने का श्रम नहीं करता कि उसके विवाहों के टूटने का कारण उसका बेहतर बनने से इनकार और जीवनसाथी से अति-अपेक्षाएं हैं।
कई मामलों में व्यवहार और दृष्टिकोण बदलने से परिवार में सचमुच चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं—सब कुछ तेज़ी से और दिखने में आसानी से सुधरता है। पर कभी-कभी एक के परिवर्तन दूसरे को रास नहीं आते—और संघ फिर भी असंगत रहता है। इसका अर्थ है—जोड़ी को अलग होना चाहिए, क्योंकि एक आत्मा प्रगति कर रही है और दूसरी हठपूर्वक सुधार से इंकार कर रही है। उसने अपने कर्मिक कार्य नहीं प्रोसेस किए हैं—और उसे यह चक्र अन्य संघों/विवाहों में फिर से, शायद कई बार, पार करना होगा।
भाग्य और कर्मिक संबंध
भाग्य को अक्सर पहले से लिखी-मोहरबंद चीज़ की तरह देखा जाता है। भाग्य मैट्रिक्स, आध्यात्मिक साधनाएं और बौद्ध धर्म कहते हैं—मनुष्य के जीवन में सब कुछ अंततः उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई मानता है कि सब पूर्वनिर्धारित है, तो वह सोच सकता है कि साथी से मिलना “भाग्य” था। पर भाग्य मैट्रिक्स कहती है—आत्मा ने कर्मिक अनुभव पाने के लिए साथी को स्वयं चुना; आप चाहें तो इसे “भाग्य” के खाते में डाल सकते हैं।
जहां कर्मिक संबंध हों—वहां प्रोसेसिंग कैसे करें
संघ को सुधारने के लिए दोनों साथियों की इच्छा आवश्यक है। दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश न करें—यह निरर्थक है और हानि पहुंचा सकती है। यदि दूसरा साथी स्थिति सुधारने के हर प्रयास का विरोध करता है, उस पर असर डालने की कोशिश झगड़ों/कांडों का कारण बन सकती है। जीवन की जड़ें और बचपन से पड़ी “सेटिंग्स” कोई और जबरन नहीं बदल सकता—कर्मिक नियतियों की प्रोसेसिंग व्यक्ति स्वयं करता है। चूंकि वैवाहिक/परिवारिक संघ में दो लोग होते हैं—परिवर्तन की चाह दोनों में होनी चाहिए। साथ ही ऐसे परिवर्तन भारी प्रयास, मनोबल, समय और लगातार कर्म-निर्वाह मांगते हैं।
यदि अलगाव/तलाक के बाद साथियों में (या एक में) पूर्व प्रिय के प्रति वितृष्णा, दावे और विवाद बचे रह जाते हैं, तो इसका मतलब—कर्मिक कार्य अधूरे हैं। इससे वही स्थिति दोहर सकती है—or वही साथी आत्मा के नए अवतार में फिर से मिल सकता है।
यदि दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि सबसे अच्छा रास्ता अलग होना है, तो एक-दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहना महत्वपूर्ण है। आखिर शुरुआत में प्रेम था—एक उज्ज्वल, यादगार भाव—और साथ रहते हुए भी बहुत कुछ अच्छा था। अलगाव के बाद भी सौहार्द विशेषतः तब आवश्यक है जब संघ में बच्चे जन्मे हों—माता-पिता उनके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, पर यह बोध कि उनके अपने लोग एक-दूसरे से घृणा करते हैं—बच्चे की मनःस्थिति पर खराब असर डालेगा। विवाह में अर्जित अनुभव शिक्षा की तरह देखा जाना चाहिए—जो अगले संघ में वही गलतियां दोहराने से रोके।
जन्मतिथियों के आधार पर कर्मिक संबंध का हिसाब
कर्मिक संबंध का आकलन करने के लिए निम्न विधियां उपयोगी हैं:
- ज्योतिष (सिनैस्ट्री—साथियों की कुंडलियों का ओवरले)।
- टैरो कार्ड का रीडिंग।
- अंकशास्त्र (न्यूमेरोलॉजी)।
- रिग्रेशन (पिछले जन्मों का अध्ययन)।
- भाग्य मैट्रिक्स।
अंतिम विधि में प्रत्येक साथी की भाग्य मैट्रिक्स की गणना की जाती है, जिसमें संबंध रेखा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और साथ ही संगतता मैट्रिक्स बनाई जाती है:
- यदि किसी भी साथी की संबंध रेखा पर आठवां आर्काना मौजूद हो—तो संबंध कर्मिक होंगे। साथी (या उनमें से एक) को पिछले अवतारों के कर्मिक कार्य प्रोसेस करने होंगे।
- दो विरोधी भूमिकाओं—जैसे “पहरेदार” और “क़ैदी”—के संघ में, निःसंकोच कहा जा सकता है कि वे यूं ही नहीं जुड़े—दोनों के कर्मिक “टेल” में वे कार्य हैं जिन्हें संघ में प्रोसेस करना है।
भाग्य मैट्रिक्स को स्वयं डिकोड करने के लिए आप वर्चुअल कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। गणना के लिए दोनों साथियों की जन्मतिथियां चाहिए।
कर्मिक संबंध और उनकी भूमिकाएं (कार्य)
भाग्य मैट्रिक्स कई अध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है, जिनमें बौद्ध धर्म भी शामिल है। बौद्ध मत में “कर्म” का अर्थ है—किसी स्पष्ट उद्देश्य/भाव के साथ किया गया कर्म। अतः कर्म/कर्मिक कार्यों की प्रोसेसिंग का मतलब है—यह जानना कि विभिन्न परिस्थितियों/कृत्यों में हमारा हेतु और विचार क्या था।
अक्सर संबंध टूटने पर व्यक्ति विनाशकारी ढंग से आचरण करता है—कल के साथी से बदला लेने, उसे चोट पहुंचाने, अपने दुखों का हिसाब चुकाने की चाह में। ऐसा ही भाव तब भी उपज सकता है जब पूर्व-साथी ने स्नेह कम दिखाया, ठंडा रहा, या कंजूस/अपमानजनक (मानसिक/शारीरिक) रहा। महत्वपूर्ण है—यह समझना कि यह विनाशकारी इच्छा—जो कर्म को बिगाड़ती है—क्यों जगी, बजाय इसके कि शांति से अलग होने, संबंध को छोड़ देने और अपने भविष्य को नकारात्मक भावों/स्मृतियों से न भरने का निर्णय लिया जाता।
पहला प्रश्न यह होना चाहिए—“मैंने अपने साथी के लिए अच्छा क्या किया?”—अधिकांश मामलों में यह प्रश्न चौंका देता है। स्पष्ट होता है—साझेदारी में मांगें तो थीं, पर सम-विनिमय नहीं। जिस कर्मिक संबंध में केवल “एकतरफ़ा यातायात” हो—वह समस्याओं के लिए अभिशप्त है, और जब संघर्ष लंबा खिंच जाए तथा शांति से सुलझाने की इच्छा न हो—तो टूट और अलगाव निश्चित है।
अपनी भाग्य मैट्रिक्स का अध्ययन करके व्यक्ति अपने कर्मों के हेतु समझ सकता है, अपनी शक्तियां/कमजोरियां जान सकता है, क्या उसे नकारात्मक कृत्यों की ओर उकसाता है—यह देख सकता है। मैट्रिक्स में कुछ स्थान लाल चिह्नित होते हैं—उन्हें विशेष ध्यान चाहिए, क्योंकि वे जीवन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों—साझेदारी/विवाह सहित—पर प्रभाव डालते हैं।
भाग्य मैट्रिक्स और संबंधों में सामंजस्य
भाग्य मैट्रिक्स जीवनयात्रियों के लिए मानचित्र और मार्गदर्शिका है—जो अपने कर्मों के कारण-परिणाम समझना चाहते हैं। यह कर्मिक संबंधों के सभी पहलुओं/विवरणों को डिकोड करती है, बताती है कि हमारे माता-पिता, हम स्वयं और हमारे बच्चों के क्या कार्य हैं—और लोग एक-दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं।
मैट्रिक्स में एक संबंध रेखा (स्वाधिष्ठान) होती है—जो संबंधों के कार्यों की व्याख्या के लिए है। प्लस ऊर्जा दिखाती है कि कर्म की प्रोसेसिंग के लिए क्या बनाए/बढ़ाए रखना है; माइनस ऊर्जा दिखाती है कि किससे बचना है और किससे लड़ना है। यदि माइनस ऊर्जाएं घटती हैं—तो कर्मिक संबंधों पर सकारात्मक असर पड़ता है—वे सुधरते हैं।
चूंकि संघ में दो लोग होते हैं—दोनों साथियों की भाग्य मैट्रिक्स का अध्ययन करना चाहिए। केवल अपनी मैट्रिक्स समझ लेने से भी व्यक्ति जीवनसाथी को नहीं समझ पाएगा; जबकि दोनों स्थिति से परिचित होंगे, तो संघ का सामंजस्य संभव होगा। हर कोई अपनी प्लस/माइनस ऊर्जाओं को जानेगा—जो पारस्परिक समझ और कुल संबंध को मजबूत करेगा।
और अच्छा तब, जब संगतता मैट्रिक्स की गणना भी हो—जो जोड़ी पर प्रभाव डालने वाली ऊर्जाओं को दर्शाती है। यह अत्यंत उपयोगी है—क्योंकि साथी न केवल संघ को बेहतर बना सकेंगे, बल्कि कर्म में “प्लस” भी पाएंगे। संभव है कि अगले जीवन में भी—उसी जोड़ी के रूप में—रिश्ते उतने ही सामंजस्यपूर्ण और प्रकाशमान हों।
भाग्य मैट्रिक्स साथियों को निम्न बातें खोलकर दिखाती है:
- संघ में संबंधों का विन्यास कैसे हो।
- आर्थिक संभावनाएं।
- संभावित समस्याएं।
- जोड़ी का एक एकक के रूप में प्रकटीकरण।
संगतता मैट्रिक्स का विश्लेषण सभी बिंदुओं पर करना चाहिए—और माइनस ऊर्जाओं से यथासंभव दूर रहना चाहिए—ताकि कर्म न बिगड़े।
मनोविज्ञान और कर्मिक नियम
बौद्ध धर्म, मनोविज्ञान, भाग्य मैट्रिक्स और कई अन्य आध्यात्मिक शिक्षाएं—कर्मिक नियमों, उनके मानवीय जीवन में स्थान और लोगों के संबंधों पर प्रभाव—की व्याख्या में लगभग एक-सी हैं। आत्मा अमर है—वह बार-बार किसी शरीर में अनुभव अर्जित करती है, कर्मिक कार्यों का अनुसरण करती है और जो पिछले जन्म में अधूरा रहा उसे पूरा करती है। साथी-चयन पर परिवार और सामाजिक परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है—जहां वह अमर आत्मा वाला व्यक्ति जीवन बिताएगा।
वंश-प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि पूर्वजों के कर्मों की निर्भरता विद्यमान है। यदि पीढ़ी-दर-पीढ़ी वंश में असुखी विवाह रहे हैं—तो इसका अर्थ है कि वंश अपने कर्मिक कार्य नहीं प्रोसेस कर रहा। सिग्मंड फ़्रायड ने कहा: “यदि एक पीढ़ी की मानसिक प्रक्रियाएं दूसरी तक न पहुंचें/जारी न रहें—तो हर किसी को जीवन फिर से सीखना पड़े—जो किसी प्रगति/विकास को असंभव बना देगा।” उनके शिष्य कार्ल युंग ने “सामूहिक अवचेतन” की अवधारणा दी। इस संदर्भ में इसका अर्थ है—हर अगली पीढ़ी की महिलाएं मां/दादी आदि का अनुभव दोहराती हैं—अर्थात अपने वंश का। आचरण के आर्कटाइप सबसे दूर के पूर्वजों से वंशानुगत होते हैं।
परंतु आर्कटाइपों और आचरण-नियमों की उपस्थिति का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति एक ही जीवन-पथ या एक ही संबंधों को अंतहीन दोहराने के लिए अभिशप्त है। यदि आत्मा बढ़ने का निश्चय करे—तो वह वंशानुगत ढर्रा तोड़ सकती है, और ऊंचे सोपानों पर चढ़ सकती है—अपने वंश के प्रति निष्ठा/बंधन बनाए रखते हुए।
आत्मा को बढ़ने में मदद करना आवश्यक है—पूर्व पीढ़ियों और अपने अनुभव का विश्लेषण करके, सही निष्कर्ष निकालकर, कारण-परिणाम को समझकर। यह सब सकारात्मक ऊर्जाओं और उच्च कंपन पर करना चाहिए। ध्यान (मेडिटेशन) समस्या के मर्म में गहन उतरने, दृश्यकरण और वंश से संबद्धताओं की समझ में सहायक है।